समाज में व्याप्त अंधविश्वास का अंधेरा? वैज्ञानिक शिक्षा,ज्ञान कसौटी पर

अंधविश्वास, यह शब्द अपने आप में ही उस अंधकार की स्मृति जगाता है जहाँ बुद्धि, तर्क और विज्ञान का प्रकाश पहुंचते-पहुंचते थक जाता है। दुर्भाग्य से हमारा समाज आज भी उसी अंधकार के कुछ कोनों में सिमटा दिखाई देता है। प्रश्न यह है कि क्या हम सचमुच इक्कीसवीं सदी के वैज्ञानिक युग में हैं, या फिर मानसिक रूप से अब भी किसी प्राचीन युग के भ्रमलोक में भटक रहे हैं?
अशिक्षा और अज्ञानता ने भारतीय समाज में अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता के बीज इतने गहरे बो दिए हैं कि वे आज वटवृक्ष बन चुके हैं। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति किसी मिथकीय धारणा या अलौकिक शक्ति पर विश्वास करता है, तो यह कुछ समय के लिए क्षम्य प्रतीत हो सकता है, पर जब शिक्षित और तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग भी बिना विचार किए इन्हीं अंधविश्वासों के पीछे भागने लगता है, तब यह हमारे समाज की बौद्धिक पतनशीलता का संकेत बन जाता है। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं, बल्कि विवेक का स्रोत है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। यही शिक्षा तर्कसंगत सोच, वैज्ञानिक दृष्टि और स्वतंत्र विचार की क्षमता प्रदान करती है। जब विज्ञान ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी चपटी नहीं, गोल है, तब मानव ने अपने विश्वास को अनुभव और प्रमाण के आधार पर बदला। यही परिवर्तनशीलता सभ्यता की पहचान है।
शहीद भगत सिंह ने अपने संगठन “नौजवान भारत सभा” के घोषणा पत्र में लिखा था — “धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरता हमारी प्रगति के सबसे बड़े शत्रु हैं।” यह वाक्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। भगत सिंह का विश्वास था कि केवल नई सोच वाले युवा ही इस रूढ़ समाज में क्रांति ला सकते हैं। उनकी यह आस्था आज भी प्रेरक है क्योंकि युवा ही वे दीपक हैं, जिनके विचारों की लौ से अंधविश्वास के अंधकार को मिटाया जा सकता है।
अंधविश्वास और आडंबर से लड़ाई का सबसे सशक्त अस्त्र शिक्षा है। शिक्षा के साथ विज्ञान और तकनीक वह दो ध्रुव हैं जिनसे होकर मनुष्य अपनी सोच को आधुनिकता की दिशा में विकसित कर सकता है। विज्ञान ने अनेकों मिथकों का भंडाफोड़ किया है, और यह सिद्ध किया है कि तर्कसंगत विचार ही सत्य की कसौटी हैं। आज जब हम चंद्रमा तक पहुँच चुके हैं, जब संचार माध्यमों ने पूरी दुनिया को एक परिवार में बदल दिया है, तब यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या बिल्ली के रास्ता काटने से सचमुच हमारा काम रुक जाता है? क्या छींकने से कोई अशुभ घटना घटती है? या फिर कौवे की बोली मेहमान का आगमन संकेतित करती है?
इन तमाम अवधारणाओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, परंतु इन पर विश्वास करना हमें तर्क से दूर और भ्रम के निकट ले जाता है। यह मनुष्य की जिज्ञासा का नहीं, बल्कि जड़ता का प्रमाण है। अंधविश्वास को सामाजिक स्वीकृति तब मिलती है जब शिक्षित व्यक्ति भी अपने विवेक का प्रयोग करना छोड़ देता है।
सबसे चिंताजनक पक्ष यह है कि आज तंत्र-मंत्र, ज्योतिष और भविष्यवाणी का कारोबार गाँवों से निकलकर महानगरों तक फैल चुका है। लोग अपने जीवन की हर समस्या का समाधान किसी तांत्रिक या “गुरु” से पूछते हैं, जो भय और विश्वास का व्यापार करते हैं। वे भूत-प्रेत, राहु-केतु या कालसर्प दोष के नाम पर भोले लोगों से धन लूटते हैं। विडंबना यह है कि इनका प्रचार अब प्रतिष्ठित टीवी चैनलों और अखबारों में भी खुलेआम होता है, मानो यह कोई वैध उद्योग हो।वास्तव में यह हमारे सामाजिक विवेक पर सबसे बड़ा प्रश्नचिह्न है। यूरोपीय देशों में भी अंधविश्वास के कुछ अंश हैं, पर वहाँ शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना ने उसकी जड़ों को कमजोर किया है। भारत में यह जड़ें इसलिए मजबूत हैं क्योंकि शिक्षा अभी भी समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुँची है।
यदि हमें सच में एक प्रगतिशील, विवेकशील और जागरूक समाज बनाना है तो प्राथमिक स्तर से ही विज्ञानसम्मत शिक्षा और आलोचनात्मक सोच को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना होगा। मीडिया और सोशल मीडिया को भी यह जिम्मेदारी निभानी होगी कि वह तर्कहीन विश्वासों के बजाय वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करे। अंधविश्वास के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई विचारों की है तर्क, शिक्षा और साहस की लड़ाई। यह युद्ध तलवार से नहीं, कलम से; आस्था से नहीं, विवेक से; अंधकार से नहीं, प्रकाश से जीता जा सकता है। हमें याद रखना होगा कि किसी भी समाज का भविष्य उसके विचारों पर निर्भर करता है, और विचार तभी विकसित होते हैं जब मनुष्य भय से मुक्त होकर प्रश्न पूछने की क्षमता रखता है।आज आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं से प्रश्न करें — क्या हम सचमुच स्वतंत्र हैं, यदि हमारे विचार अब भी जंजीरों में जकड़े हैं? क्या यह आधुनिकता केवल तकनीकी है, या मानसिक भी? यदि उत्तर “नहीं” है, तो हमें स्वयं को पुनः शिक्षित करना होगा।
अंधविश्वास से मुक्त समाज वही होगा जहाँ तर्क, ज्ञान और सत्य का सम्मान होगा। वह दिन ही सच्चे अर्थों में “नवजागरण” का दिन होगा — जब मनुष्य अपने मस्तिष्क की स्वतंत्रता को धर्म, परंपरा या भय के किसी बंधन से मुक्त कर पाएगा।
संजीव ठाकुर,


 वेटरन्स डे
वेटरन्स डे  ‘भजन-राज’ यानी ‘भरोसे के शासन’ में राजस्थान के नये आयाम -ललित गर्ग-
‘भजन-राज’ यानी ‘भरोसे के शासन’ में राजस्थान के नये आयाम -ललित गर्ग-  बचत और खर्च का असंतुलनः नये भारत के लिए बड़ी चुनौती -ललित गर्ग-
बचत और खर्च का असंतुलनः नये भारत के लिए बड़ी चुनौती -ललित गर्ग- 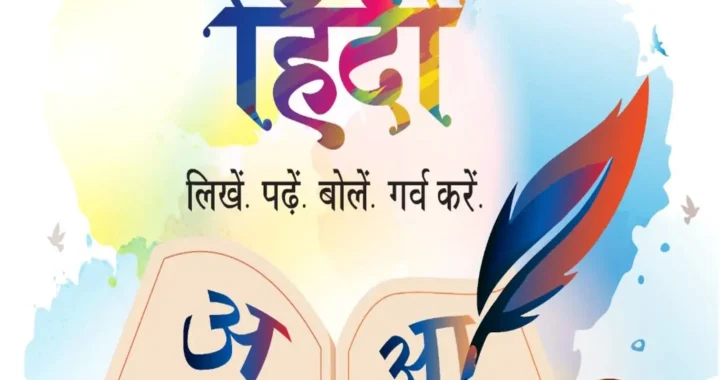 विश्व में हिन्दी की बढ़ती साखः भारत में उपेक्षा क्यों? -ललित गर्ग-
विश्व में हिन्दी की बढ़ती साखः भारत में उपेक्षा क्यों? -ललित गर्ग-  दुुनिया में मंदीः भारत में आर्थिक मजबूती की रोशनी -ललित गर्ग-
दुुनिया में मंदीः भारत में आर्थिक मजबूती की रोशनी -ललित गर्ग-  जिन्ना का पाकिस्तान इंटरनेशनल मोनेटरी फंड के सामने नतमस्तक, बेबस जनता खाने को तरस रही है
जिन्ना का पाकिस्तान इंटरनेशनल मोनेटरी फंड के सामने नतमस्तक, बेबस जनता खाने को तरस रही है 