धनतेरस धन के भौतिक एवं आध्यात्मिक समन्वय का पर्व -ललित गर्ग-

धनतेरस- 18 अक्टूबर, 2025
धनतेरस का पर्व पंच दिवसीय दीपोत्सव की पवित्र श्रृंखला का आरंभिक द्वार है। यह केवल सोना-चांदी, वस्त्र या बर्तन खरीदने का शुभ दिन नहीं, बल्कि धन के प्रति हमारी सोच को पुनर्संतुलित करने का अवसर है। भारतीय संस्कृति में धन को सदैव देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, परंतु यह पूजन केवल भौतिक संपदा का नहीं, बल्कि धन के नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उपयोग का भी प्रतीक है। ऋषि-मुनियों ने धन को केवल मुद्रा नहीं, बल्कि एक ऊर्जा माना है। उपनिषदों में कहा गया है-“धनं मूलं सर्वेषां साधनानाम्”, अर्थात धन सभी साधनों का मूल है, परंतु वही धन शुभ है जो धर्म-संयम से अर्जित और लोककल्याण में नियोजित हो। धनतेरस हमें याद दिलाता है कि धन केवल संग्रह का नहीं, उपयोग का विषय है। धन का सही उपयोग ही उसे ‘लक्ष्मी’ बनाता है, अन्यथा वह ‘अलक्ष्मी’-अशांति और विषमता का कारण बन जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस तिथि को धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बर्तन, सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। ऐसे में यह दिन धन्वंतरि को समर्पित किया गया है।
भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन कहा गया है। भगवान धन्वंतरि को भगवान विष्णु का अंश माना गया है, जिन्होंने मानव समाज को चिकित्सा विज्ञान (आयुर्वेद) का ज्ञान दिया। इसी कारण धनतेरस के दिन देशभर में वैद्य समाज भगवान धन्वंतरि जयंती के रूप में उनकी पूजा करता है। धनतेरस का ऐतिहासिक महत्व समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है, जब भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इसे ‘धनत्रयोदशी’ भी कहते हैं। यह त्योहार भगवान धन्वंतरि को समर्पित है, जिन्हें आयुर्वेद और चिकित्सा का देवता माना जाता है, और धन एवं समृद्धि के देवता भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ इस दिन यम दीपक जलाने का भी विधान है। जिसे दीपदान भी कहा जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार, यमराज से अपनी रक्षा करने के लिए इस दिन यमदीपदान किया जाता है। एक कथा के अनुसार, एक राजा के पुत्र को साँप के काटने से मृत्यु होने की भविष्यवाणी थी, जिसे उसकी पत्नी ने दीप और सोने-चाँदी के ढेर लगाकर यमराज को दूर रखने में सफल हुई। जैन आगम में धनतेरस को ‘धन्य तेरस’ या ‘ध्यान तेरस’ भी कहते हैं।
प्राचीन भारत में धन का वितरण और उपयोग धर्म और नीति के साथ जुड़ा हुआ था। व्यापारी ‘लाभ’ में भी ‘लोक-लाभ’ देखते थे। राजा अपने धन को जनकल्याण, सिंचाई, शिक्षा और सुरक्षा में लगाते थे। किन्तु आधुनिक युग में, विशेषतः पूंजीवादी व्यवस्था के प्रसार के बाद, धन का स्वरूप विकृत हुआ है। धन साधन से लक्ष्य बन गया है। इसके परिणामस्वरूप समाज में अमीरी-गरीबी की खाई, शोषण, और भ्रष्टाचार बढ़ा है। आज एक ओर अरबपतियों की गिनती बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों लोग रोटी और दवा के अभाव में जीवन गुज़ार रहे हैं। धनतेरस का पर्व इस विडंबना पर आत्ममंथन का अवसर है। यह हमें पुकारता है कि हम धन को केवल अपनी तिजोरी का नहीं, बल्कि समाज की समृद्धि का माध्यम बनाएं। लोकमान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन (वस्तु) खरीदने से उसमें तेरह गुणा वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनियाँ के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग-बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन चाँदी खरीदने की भी प्रथा है, चांदी शुद्धता की प्रतीक है यहीं शुद्धता इंसानी जीवन में आये, यही इस पर्व का उद्घोष है।
महात्मा गांधी ने कहा था-“पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, परंतु जब वह मनुष्य का स्वामी बन जाता है, तब वह विनाश का कारण बनता है।” धनतेरस का सच्चा संदेश यही है-धन का स्वामी बनो, उसका दास नहीं। धन के प्रति सकारात्मक दृष्टि का अर्थ है उसे साधना, सेवा और संस्कार से जोड़ना। आज आवश्यकता है कि हम धन को साझा समृद्धि, सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीय करुणा के उपकरण के रूप में देखें। आज विश्व अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती समान अवसरों का अभाव है। धनतेरस का यह अवसर सरकारों को भी यह संदेश देता है कि वे विकास के लिए धन का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करें। राजकोषीय नीतियाँ केवल अमीर वर्ग के लाभ के लिए नहीं, बल्कि गरीबों के सशक्तिकरण एवं कल्याण के लिए हों। धन की प्रवाह प्रणाली में नैतिकता, पारदर्शिता और संवेदना का समावेश आवश्यक है।
आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने भी धन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। उन्होंने भगवान महावीर के आर्थिक दर्शन को आधुनिक संदर्भों में व्याख्यायित करते हुए ‘महावीर का अर्थशास्त्र’ नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। आचार्य महाप्रज्ञ ने स्पष्ट किया कि धन का अर्जन और उपयोग दोनों ही अहिंसक, नैतिक और संयमित होने चाहिए। उनके अनुसार धन तभी सार्थक है जब वह आत्मविकास, समाजकल्याण और न्यायपूर्ण व्यवस्था का साधन बने। उन्होंने महावीर के अर्थशास्त्र में बताया कि “धन की मर्यादा उसका त्याग नहीं, उसका संयम है।” यह विचार धनतेरस के मूल भाव को ही पुष्ट करता है कि धन को नकारा नहीं जाए, बल्कि उसे लोकमंगल में प्रवाहित किया जाए।
धनतेरस का अर्थ केवल भौतिक संपत्ति का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सद्गुण और आत्मबल का भी प्रतीक है। आयुर्वेद में इसी दिन धन्वंतरि जयंती भी मनाई जाती है, जो चिकित्सा और स्वास्थ्य के देवता हैं। इस परंपरा में धन का अर्थ केवल पैसा नहीं, बल्कि आरोग्य, अन्न, शिक्षा और शांति भी है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि धन और धर्म का संवाद पुनः स्थापित हो। धर्म के बिना धन अंधा है, और धन के बिना धर्म असहाय। धनतेरस हमें सिखाता है कि धन का अर्जन सत्य मार्ग से हो और उसका उपभोग सेवा मार्ग पर हो। आचार्य तुलसी ने अर्जन के साथ विसर्जन का सूत्र दिया, यानि अर्जन के साथ जनकल्याण के लिये विसर्जन का क्रम चले। मनुस्मृति में कहा गया है-“धनं धर्मेण संचिनुयात्”, अर्थात धन का संचय धर्म के मार्ग से ही किया जाना चाहिए।
धनतेरस केवल सोना-चांदी खरीदने का दिन नहीं, बल्कि धन की शुद्धता और सदुपयोग की तपश्चरण का पर्व है। इस तरह से धनतेरस का पर्व केवल धन प्राप्ति का नहीं बल्कि आरोग्य, आयु और समृद्धि की कामना का पर्व है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि असली संपत्ति हमारा स्वास्थ्य है। इसलिए इस दिन की पूजा न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि जीवन के संतुलन और सुख-शांति का भी प्रतीक है। आज जब समाज में धन के कारण विभाजन, भ्रष्टाचार और अन्याय बढ़ रहे हैं, तब धनतेरस हमें प्रेरित करता है-धन को ‘दिव्यता’ में रूपांतरित करने की। यह पर्व हमें पुकारता है कि हम धन के प्रति अपनी दृष्टि बदलें-धन को नकारें नहीं, बल्कि उसे साकार करें; धन से मोह न रखें, परंतु उसे लोकमंगल में प्रवाहित करें। जब धन का प्रवाह धर्म के संग बहता है, तभी सच्चा दीपोत्सव जगमगाता है-अंतर में भी, समाज में भी, और मानवता में भी।


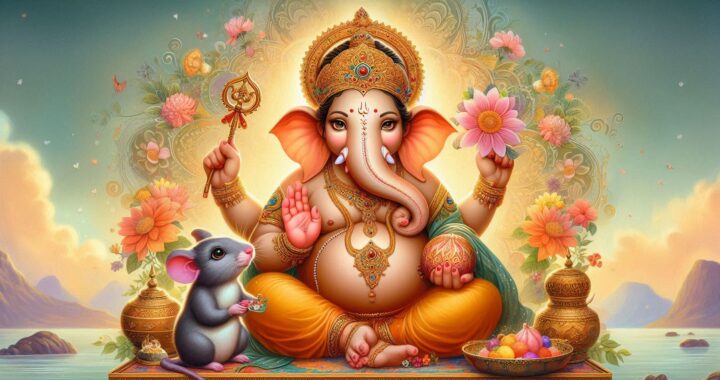 गणेश हैं विघ्नहर्ता- एवं जीवंत राष्ट्रीयता के प्रतीक -ललित गर्ग-
गणेश हैं विघ्नहर्ता- एवं जीवंत राष्ट्रीयता के प्रतीक -ललित गर्ग-  गुरु जीवनरूपी अंधेरों को मिटाकर उजाला करते हैं -ललित गर्ग-
गुरु जीवनरूपी अंधेरों को मिटाकर उजाला करते हैं -ललित गर्ग-  नवदुर्गा में मां की आरती पूजा अर्चना के साथ मेले का हुआ आयोजन
नवदुर्गा में मां की आरती पूजा अर्चना के साथ मेले का हुआ आयोजन  शांति, संस्कृति एवं शिक्षा का महापर्व है बसंत पंचमी -ः ललित गर्ग:-
शांति, संस्कृति एवं शिक्षा का महापर्व है बसंत पंचमी -ः ललित गर्ग:-  सूर्य के उत्तरायण में आगमन का खगोलीय पर्व है मकर सक्रांति — डॉ श्रीगोपाल नारसन एडवोकेट
सूर्य के उत्तरायण में आगमन का खगोलीय पर्व है मकर सक्रांति — डॉ श्रीगोपाल नारसन एडवोकेट  मधु कैटभ को दिए वरदान को पूरा करने मकर संक्रांति के दिन मंदार आते हैं भगवान भधुसूदन — कुमार कृष्णन
मधु कैटभ को दिए वरदान को पूरा करने मकर संक्रांति के दिन मंदार आते हैं भगवान भधुसूदन — कुमार कृष्णन 