इस्राइल-हमास युद्धविरामः आशा की किरण या अस्थायी विराम? – ललित गर्ग –

गाज़ा की धरती लम्बे दौर से संघर्ष, हिंसा, विनाश और तबाही की त्रासदी की गवाह रही है, आज फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ शांति की एक हल्की किरण दिखाई तो देती है, परंतु उसके चारों ओर धुएँ और राख का अंधकार अब भी विद्यमान है। हाल ही में हुए युद्ध-विराम ने न केवल मध्यपूर्व बल्कि समूचे विश्व को राहत की एक साँस दी है। गाजा में अमन-चैन की ओर जो सुखद कदम बढ़े हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। परंतु यह सवाल भी उतना ही प्रासंगिक है कि क्या यह शांति स्थायी होगी, या यह केवल अगली लड़ाई से पहले का ठहराव भर है? समूची दुनिया चाहती है कि यह युद्ध विराम स्थायी हो क्योंकि इस्राइल और हमास के संघर्ष ने करीब बाइस लाख से अधिक लोगों को बेघर करके भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। ऐसे में दोनों पक्षों के लिये समझौते के पहले चरण को पूरी तरह से लागू करना बेहद जरूरी होगा। जिसमें बंधकों व कैदियों की रिहाई, गाजा में मानवीय सहायता को अनवरत जारी रखना और इस्राइली सेनाओं की गाजा के मुख्य शहरों से आंशिक वापसी सुनिश्चित करना भी शामिल है। यह सब दूसरे चरण की बातचीत पर निर्भर हैं।
यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो इसके बाद ही दूसरे चरण की बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह बेहद मुश्किल चुनौतियों वाला चरण होगा। इस दौरान कई संवेदनशील मुद्दे सामने होंगे। सबकी निगाह इस पर होगी कि शांति समझौते के अगले चरण कब पूरे होते हैं और वे सही तरह पूरे होते भी हैं या नहीं? इस पर संशय इसलिए है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं कि इजरायली सेना गाजा में कितना पीछे हटेगी और वहां के प्रशासन को संचालित करने का कैसा तंत्र तैयार होगा और क्या उस पर हमास सहमत होगा? इसके अतिरिक्त जहां हमास को हथियार छोड़ने हैं, वहीं इजरायल को स्वतंत्र फिलस्तीन देश की राह आसान करनी है। हमास का कहना है कि हथियार तब छोड़े जाएंगे, जब स्वतंत्र फिलस्तीन का रास्ता साफ होगा। इस पर इजरायल तैयार नहीं दिख रहा है। यह ठीक है कि स्वयं की ओर से प्रस्तावित गाजा शांति समझौते पर अमल शुरू होने के अवसर पर मिस्र जाने के पहले इजरायल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी पहल को पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना का पथ करार दिया और इजरायली प्रधानमंत्री से ईरान से समझौता करने को कहा। ऐसे किसी समझौते की सूरत तब बनेगी, जब ईरान इजरायल को मिटाने की अपनी जिद छोड़ेगा।
गाज़ा की वर्तमान स्थिति किसी एक राष्ट्र या एक नीति की देन नहीं है; यह दशकों से चली आ रही अविश्वास, असमानता और राजनीतिक स्वार्थों की परिणति है। इस बार के संघर्ष ने जिस तरह से निर्दाेष नागरिकों, बच्चों और महिलाओं को अपना शिकार बनाया, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि युद्ध चाहे किसी भी नाम पर लड़ा जाए, उसका परिणाम हमेशा मानवीय त्रासदी ही होता है। अस्पताल, विद्यालय, धार्मिक स्थल-कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं रहा। अमेरिकी मध्यस्थता वाले युद्धविराम समझौते के बाद हमास ने आखिरकार शेष जीवित बचे बीस इस्राइली बंधकों को रिहा कर दिया। जिसके बाद इस्राइल में किसी बड़े उत्सव जैसा जश्न दिखा। बहरहाल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी भी इस्राइल-हमास जोखिमभरा युद्धविराम समझौता नाजुक बना हुआ है। इसकी वास्तविक परीक्षा आने वाले दिनों में होगी। इस संघर्षरत क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिये जरूरी है कि प्रमुख हितधारकों की ओर से गंभीर एवं ईमानदार प्रयास लगातार होते रहें। वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती भूतहा खण्डहर एवं तबाही में तब्दील हो चुके गाजा के पुनर्निर्माण की होगी। दो साल से लगातार जारी युद्ध के चलते यह इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है।
एक नाजुक समय में जब युद्धविराम की घोषणा हुई, तो यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं है, बल्कि मानवीय विवेक का पुनर्जागरण भी है। यह समझना आवश्यक है कि शांति कोई समझौता नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता है। यही कारण है कि यह युद्धविराम पूरी मानवता के लिए एक ‘आशा की किरण’ बनकर उभरा है। यह उस संभावना का प्रतीक है कि जब दुनिया के शक्तिशाली देश, विशेषकर अमेरिका, यूरोप, और अरब राष्ट्र अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं से ऊपर उठकर मानवीय सरोकारों को महत्व देते हैं, तो समाधान की दिशा में रास्ता बनता है। फिर भी इस शांति की वास्तविकता पर प्रश्नचिह्न बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही इस युद्धविराम को अपने कूटनीतिक प्रयासों की उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया हो, पर सच यह है कि युद्ध तब रुका जब उसकी भयावहता अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। यह विराम किसी की “कूटनीति की जीत” से अधिक, मानवीय विवशता की उपज है। अंतरराष्ट्रीय दबाव, मानवीय संगठनों की सक्रियता और आम नागरिकों की पुकार ने मिलकर इस विराम को संभव बनाया। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह शांति टिके, युद्ध का अंधेरा नहीं, शांति का उजाला फैले। क्योंकि जब तक गाज़ा के लोगों को जीवन की मूलभूत सुविधाएँ-पानी, भोजन, दवा, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन नहीं मिलते, तब तक शांति केवल कागज़ों पर दर्ज रहेगी। वास्तविक शांति केवल तब संभव है जब अन्याय, दमन और असमानता के ढाँचे टूटें। शांति का अर्थ केवल हथियारों का मौन नहीं, बल्कि हृदयों का परिवर्तन है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए गाजा शांति समझौते को पश्चिम एशिया की ऐतिहासिक सुबह की संज्ञा दी। वे कुछ भी दावा करें, फिलहाल यह कहना कठिन है कि प्रमुख मुस्लिम देश इजरायल को मान्यता देने के लिए तैयार होंगे। भले ही ट्रंप यह कह रहे हों कि गाजा शांति समझौते को सभी मुस्लिम देशों का समर्थन मिला, लेकिन वस्तुस्थिति इससे अलग है। जब यह समझौता सामने आया था, तब उसे समर्थन देने और ट्रंप की प्रशंसा करने वालों में पाकिस्तान भी था, पर अब वह इस समझौते को समर्थन देने से केवल पीछे ही नहीं हट गया, बल्कि उसने अपने यहां ऐसा माहौल बनाया कि उसके विरोध में कट्टरपंथी तत्व सड़क पर उतर आए। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि पाकिस्तान ने गाजा शांति समझौते को नकारने के लिए ही कट्टरपंथी तत्वों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया और फिर उन पर गोलियां भी चलवाईं, ताकि दुनिया और विशेष रूप से अमेरिका को यह संदेश जाए कि उसके लिए गाजा शांति समझौते को स्वीकार करना संभव नहीं। यहां अमेरिका को पाक के दोहरे चरित्र को समझ लेना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, अरब लीग और विश्व की सभी बड़ी शक्तियों की जिम्मेदारी है कि वे इस युद्धविराम को केवल घोषणा भर न रहने दें। उसे स्थायी बनाने के लिए एक ठोस मानवीय पुनर्निर्माण योजना तैयार की जाए, जिसमें राजनीतिक समाधान, मानवीय सहायता और संवाद-तीनों को समान महत्व मिले। गाज़ा के बच्चे जब फिर से स्कूलों में लौटेंगे, जब शरणार्थी अपने घरों में बस सकेंगे, जब भय की जगह भरोसा जन्म लेगा, तभी यह कहा जा सकेगा कि गाज़ा में शांति आई है। इजरायल को यहां ज्यादा उदारता का परिचय देना होगा, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह बहुत ताकतवर है। हमास को भी हिंसा से बचना चाहिए। द्वि-राष्ट्रीय व्यवस्था को जमीन पर ठीक से साकार करना हमास का लक्ष्य होना चाहिए । हमास को अपनी छवि सुधारने की चिंता करनी चाहिए, अगर उस पर यकीन किया गया है, तो उसे खरा उतरना होगा। गाजा में किसी भी सूरत में हिंसा की वापसी नहीं होनी चाहिए। आज यह युद्धविराम भले ही ‘एक आशा की किरण’ बना हो, परंतु उसे स्थायी प्रकाश में बदलना विश्व समुदाय के विवेक, संवेदनशीलता और सतत प्रयास पर निर्भर करता है


 एसआईआर का विरोधः चिन्ता लोकतंत्र की या वोट बैंक की? -ललित गर्ग-
एसआईआर का विरोधः चिन्ता लोकतंत्र की या वोट बैंक की? -ललित गर्ग-  साहित्यकार कवि लेखक संजीव ठाकुर को राष्ट्रीय तुलसी साहित्य अकादमी द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार एवं प्रांत अध्यक्ष मनोनीत किया गया
साहित्यकार कवि लेखक संजीव ठाकुर को राष्ट्रीय तुलसी साहित्य अकादमी द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार एवं प्रांत अध्यक्ष मनोनीत किया गया 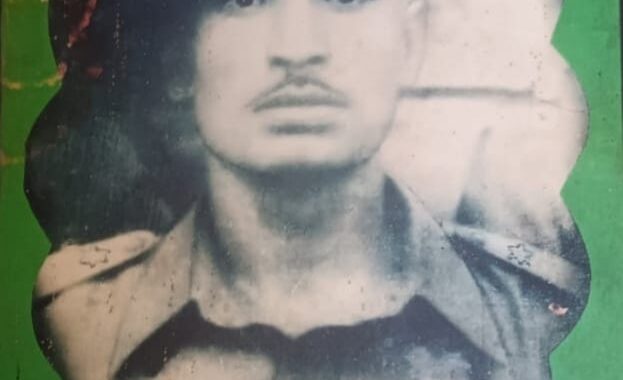 नायब सुबेदार माम चन्द्र शर्मा , वीर चक्र (मरणोपरान्त)
नायब सुबेदार माम चन्द्र शर्मा , वीर चक्र (मरणोपरान्त)  हिंदी में शपथः नए भारत की भाषाई चेतना का निर्णायक उद्घोष -ललित गर्ग-
हिंदी में शपथः नए भारत की भाषाई चेतना का निर्णायक उद्घोष -ललित गर्ग-  संविधानः लोकतंत्र की आत्मा और सुशासन का आधार -ललित गर्ग-
संविधानः लोकतंत्र की आत्मा और सुशासन का आधार -ललित गर्ग-